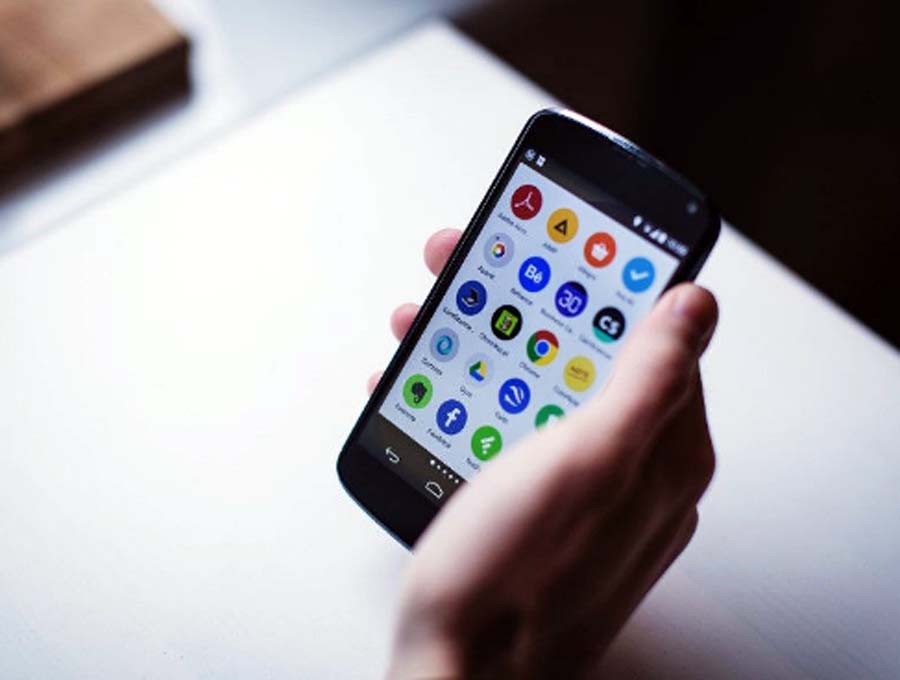इसी माह देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा। चूंकि एक सांसद के रूप में अटल जी का आचरण अविस्मरणीय है लेकिन जिस तरह गत दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में जो कुछ हुआ वह अटल जी को जरूर निराश करेगा। गत दिनों शीतकालीन सत्र का समापन हो गया, लेकिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियां हंगामें की भेंट चढ़ी, जोकि एक गंभीर चिंता का विषय है।
अगर 16वीं लोकसभा के गठन के बाद से संसद के अभी तक के सभी सत्रों पर नजर डाली जाए, तो यह शीतकालीन सत्र सर्वाधिक निराश करने वाला साबित हुआ। 16 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक चलने वाले इस सत्र में लोकसभा ने महज 15 फीसदी तो राज्यसभा ने केवल 18 फीसदी काम किया। संसद की उत्पादकता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार केवल 2 विधेयक ही पारित हो सके जबकि 8 विधेयकों को प्रस्तुत किया गया था। संसद ने नोटबंदी से उभरी तमाम समस्यायों पर कोई चर्चा नहीं की, जम्मू-कश्मीर में आये दिन शहीद हो रहे जवानों पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, यदि हंगामा हुआ तो सिर्फ इस बात को लेकर कि मोदी संसद में क्यों नहीं बोलते और नोटबंदी पर चर्चा नियम 184 के तहत हो या नियम 193 के तहत।
दरअसल नियम 184 के तहत चर्चा के पश्चात मतदान होता है, जिससे सरकार के प्रति संसद का मिजाज स्पष्ट होता है और सरकार को घेरने का मौका भी मिल जाता है जबकि नियम 193 में सिर्फ चर्चा ही होती है मतदान नहीं। चर्चा किस नियम के अंतर्गत हो इस पर अंतिम निर्णय स्पीकर का ही होता है, परन्तु बहुमत के चलते अप्रत्यक्ष रूप से सरकार निर्णय करने में अपनी भूमिका रखती है। संसद के शीतकालीन सत्र में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? चाहे उंगलियां विपक्ष पर खड़ी हों या सरकार पर लेकिन अंतत: इससे देश की जनता ही प्रभावित होती है. सरकार पर देश चलाने का जिम्मा होता है और विपक्ष पर पहरेदारी का, देश लाइन में लगा है, नोटबंदी से समस्या विकराल होती चली गयी लेकिन सरकार और विपक्ष चर्चा के लिए किसी सर्वमान्य हल पर ही नहीं पहुंच पाए। संसद के इस रवैय्ये से लालकृष्ण अडवानी भी असहमत दिखे और उन्होंने कहा कि यदि आज अटल जी संसद में होते तो वह काफी निराश होते।
दरअसल सवाल यह है कि सत्र-दर-सत्र मजबूत हो रही हंगामे की परिपाटी को कैसे तोड़ा जाए? कैसे संसद को जवाबदेह और किसके लिए जवाबदेह बनाया जाए? संसदीय शासन प्रणाली में सरकार संसद के लिए जवाबदेह होती है, संसद प्रश्न और प्रस्ताव के जरिये उस पर नियंत्रण रखती है लेकिन संसद में विपक्ष और सरकार के अहं का टकराव चरम पर है, जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ हंगामे के रूप में सामने आता है।
संविधान का अनुच्छेद 122 संसद को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान करता है। भारत में न्यायिक सक्रियता आज जिस चरम पर है वह कार्यपालिका की निष्क्रियता का ही परिणाम है और अब विधायिका जिस निष्क्रियता पर उतारू है उससे तो यही लगता है कि लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कहीं न्यायपालिका को संसदीय आचरण पर भी हस्तक्षेप न करना पड़े। क्योंकि यदि संसद में हंगामे की परिपाटी नहीं टूटी तो यह जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या होगी और जब संसद ही असंवैधानिक व्यवहार पर उतारू हो जाए तो जनता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता क्योंकि वह सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को चुनने तक ही अपनी भूमिका रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे इस परिपाटी को बदला जाए।
इस सन्दर्भ में बीजद सांसद बैजयन्त पांडा ने एक आलेख के जरिये संसदीय नियमों में परिवर्तन का सुझाव दिया था। उनके सुझाव बेहद प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। पांडा के अनुसार हमारी संसदीय व्यवस्था में कुछ नियम बहुत ही अस्पष्ट प्रतीत होते हैं। यदि स्पीकर की शक्तियों में वृद्धि कर दी जाए व सांसदों द्वारा हंगामे की स्थिति में दंड सम्बन्धी प्रावधान कठोर किये जाएं, तो हंगामे की परिपाटी को तोड़ा जा सकता है। दरअसल स्पीकर को यह शक्ति स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए कि वह हंगामा करने की स्थिति में किसी सदस्य को अनिश्चित कालीन समय के लिए सदन से निलंबित कर सके। और दंड की यह परिपाटी मजबूत की जाए ताकि सदन में अनुशासन स्थापित किया जा सके।
दरअसल हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रभावित है और आज भी हमारी संसद उन संसदीय नियमों का पालन कर रही है जिन्हें खुद ब्रिटेन की संसद समाप्त कर चुकी है। आज नियम 184 के तहत चर्चा को लेकर जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, वह नया नहीं हैं पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में भी ऐसा ही गतिरोध पैदा होता था। चूंकि संसद अपनी प्रक्रियायों के लिए नियम स्वयं बनाती है, इसलिए संसदीय नियमावली में संसद को संसोधन करके स्पष्ट करना चाहिए कि किन मामलों में नियम 184 के तहत चर्चा होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि यदि 150 सांसद स्पीकर को लिखित रूप में आवेदन करें, तो उसे नियम 184 के तहत चर्चा कराने के लिए बाध्य होना पड़े। यदि 150 सांसदों के आवेदन सम्बन्धी बाध्यता को लागू कर दिया जाता है तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं जो कार्यवाहियों में बाधक बनती हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।
संसदीय अनुशासन हीनता जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था की छवि खराब करती है वहीं यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक सिद्ध होती है। संसद कानून बनाकर समाज को भिन्न रूपों में प्रभावित करती है। जिसका सकारात्मक प्रभाव देश की जीडीपी पर पड़ता है। दरअसल विधायन प्रक्रिया से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होता है। सामान्यत: संसद की कार्यवाहियों का मौद्रिक आंकलन ही किया जाता है लेकिन हम कई ऐसे कदमों का आंकलन नहीं कर पाते जो किसी न किसी रूप में देश के लिए लाभकारी सिद्ध होते। गत शीतकालीन सत्र में जो भी हुआ उसे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति मानकर सभी दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि इस तरह का असंवैधानिक और असंसदीय आचरण लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। यह देश के छवि और व्यवस्था दोनों के लिए ही चुनोतिपूर्ण है।
पार्थ उपाध्याय
Create an account
Welcome! Register for an account
A password will be e-mailed to you.
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Trending Now