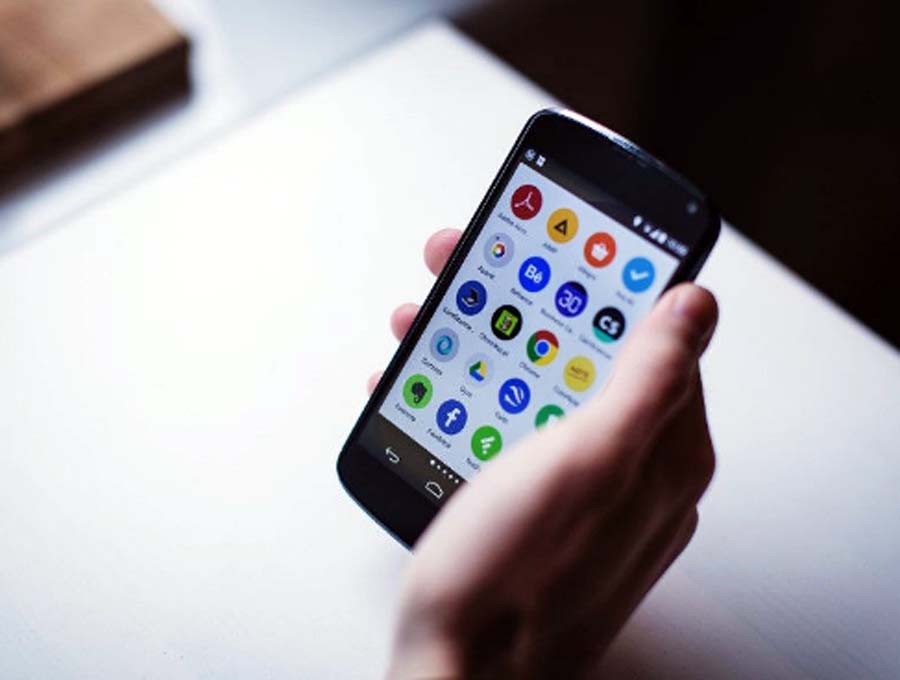किसी भी देश के साक्षरता प्रतिशत का अच्छा होना उस देश के विकास और सम्पन्नता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने की योग्यता से है जबकि अक्षरों का ज्ञान न होना निरक्षता कहलाता है। पुराना समय साधारण और सरल था। तब न तो जीवन इतना गतिशील था और न ही जीवन जीने के साधन इतने जटिल थे। जरूरत बहुत सीमित थीं। दो जून की रोटी कमाकर व्यक्ति चैन की नींद सो जाता था। अब इच्छाओं और आकांक्षाओं ने आकाश की सीमाओं को चुनौती दी है।
ऐसे में अनपढ़ व्यक्ति न तो तेज रफतार युग के साथ चल पायेगा और न ही उसकी सोच की सीमा विस्तृत होगी। साक्षरता मानव विकास की आधारशिला है। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व हमारे देश की जनसंख्या में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। किन्तु सरकार के अथक प्रयासों से आज समाज हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अनपढ़ व्यक्ति ज्ञान और जानकारी के अथाह भंडार से वंचित रह जाता है। और वह कुएँ के मेढक के समान अपनी संकीर्ण दुनिया में ही कैद रह जाता है। वह न तो अधिकारों का सही प्रयोग और न ही जनसामान्य के लिए उपलब्ध सुख-सुविधाओं का लाभ उठा पाता है।
आज की आधुनिक युग में निरक्षरता एक दुर्गुण बन गया है। घर घर और गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे की हर व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में उन्नति हो। वह अंगूठा छाप न रहे, उसे कोई ठग न सके। हर वर्ग का व्यक्ति अपनी अच्छाई बुराई समझे और अपनी दैनिक जीवनचर्या में सूझ बूझ के साथ फैसला ले। उसे अंधविश्वासों और शोषण से मुक्ति मिले। जहां शिक्षा एक वरदान है तो वही निरक्षरता एक अभिशाप की तरह है। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए साक्षर होना उतना ही अनिवार्य है जितना एक अंधे के लिए आँखे।
वर्तमान सभ्यता काफी उन्नत हो चुकी है ईस उन्नति का एक मुलभुत आधार है शिक्षा। शिक्षा के बिना प्रगति का पहिया एक इंच भी नहीं सरक सकता। आज निरक्षर लोगों को ज्ञान-विज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है उसे पत्र पढ़ने, बस रेलगाड़ी की सूचनाये पढने के लिए भी लोगो का मुहँ ताकना पड़ता है। निरक्षर होने का सीधा-सरल अर्थ है अनपढ़ होना।
काला अक्षर भैंस बराबर यह कहावत अनपढ़ व्यक्ति के लिए ही प्रयोग की जाती है। अर्थात अनपढ़ व्यक्ति को काले अक्षर और भैंस में कोई अन्तर नजर नहीं आता। आज का युग विज्ञान का युग है। लोग अपने-अपने काम में इतना व्यस्त हो गये हैं कि एक दूसरे को किसी विषय में मौखिक जानकारी देने के लिए उनके पास अधिक समय नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को जानकारी देने के लिए हर जगह अनेक बातें लिख दी जाती हैं। वह चाहे दुकानों के साइनबोर्ड हों या रेलवे की समय-सारण का चार्ट।
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा और यूनिस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा 287 लाख अशिक्षित वयस्कों की संख्या है। ये आँकड़े देश में शिक्षा के क्षेत्र में चौका देने वाली असमानता की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 1991 से 2006 तक अशिक्षा का स्तर 63 फीसदी तक बढ़ा है। एक उच्च साक्षरता किसी भी राष्ट्र को वैश्विक मंच पर अन्य राष्ट्रों के साथ बराबरी पर लाने के लिये अनिवार्य आवश्यकता होती है।
कोई भी राष्ट्र नीची साक्षरता दर के साथ होनहार राष्ट्र नहीं माना जाता। इसके अलावा इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि भारत वो देश है जहाँ असमानता इस हद तक है कि एक राज्य ने 90 फीसदी से ज्यादा साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी है जहाँ साक्षरता दर अभी भी निराशाजनक है।
भारत मे अशिक्षा एक समस्या है जो इससे जटिल आयामों के साथ जुड़ी हुई है। भारत में अशिक्षा उन विभिन्न असमानताओं के आयामों में से एक है जो देश में अस्तित्व में है। यहां लिंग असमानता, आय असमानता, राज्य असंतुलन, जाति असंतुलन और तकनीकी बाधाएं है जो देश में साक्षरता की दर को निर्धारित करती है। भारत के पास सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 82.14 फिसदी और महिलाओं की साक्षरता 65.46 फिसदी है।
कम महिला साक्षरता भी लिखने और पढ़ने की गतिविधियों के लिये महिलाओं के पुरुषों पर निर्भर रहने के लिये जिम्मेदार है। इस प्रकार इसने एक दुष्चक्र का रुप ले लिया है। निराशाजनक साक्षरता दर का मुख्य कारणों में से एक स्कूलों की अपर्याप्त सुविधा है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ अक्षम और अयोग्य है।
1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार 83वें संवैधानिक संशोधन 2000 के तहत वर्ष 2003 में संविधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल किया गया। इसके बावजूद भी देश 10-14 साल की आयु वाले बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान नहीं कर सका।
देश में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये बहुत सी अन्य योजनाओं को भी लागू किया गया। जैसे 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 1992 की शिक्षा नीति और फिर 2001 में 6 से 14 साल तक की आयु वाले सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और 2010 तक स्कूल में आठ साल पूरे करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था।
ये सभी ऐसी नीतियाँ हैं जो आज धूल फाँक रही है। क्योंकि ये प्रचलित अशिक्षा और बच्चों को स्कूल में लाने और रोकने में सक्षम नहीं हो पायी हैं। न केवल सरकार परन्तु हर शिक्षित व्यक्ति को निरक्षरता के उन्मूलन को व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। सभी शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया गया हर एक प्रयास इस खतरे से निजात में सहयोग कर सकता है। इस नेक कार्य में जनता की भागीदारी आवश्यक है।
भरत यादव
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।